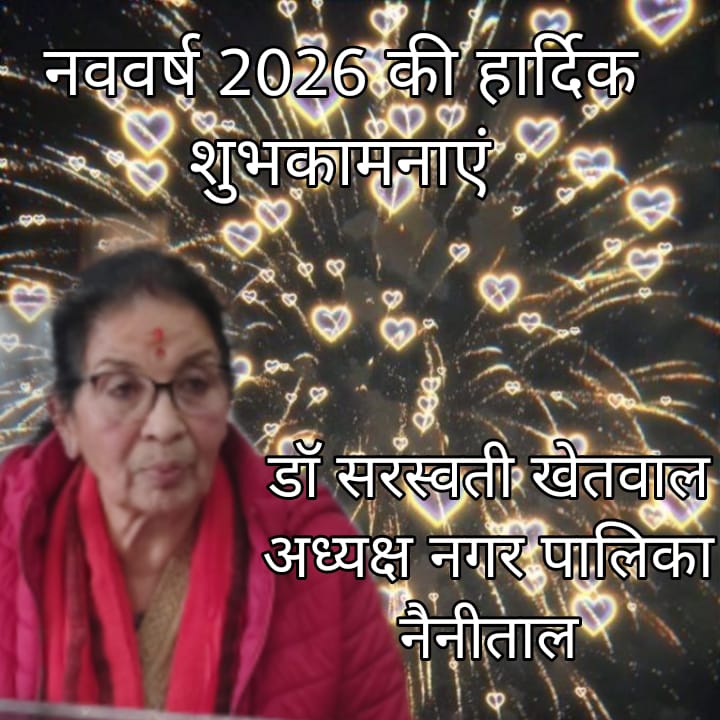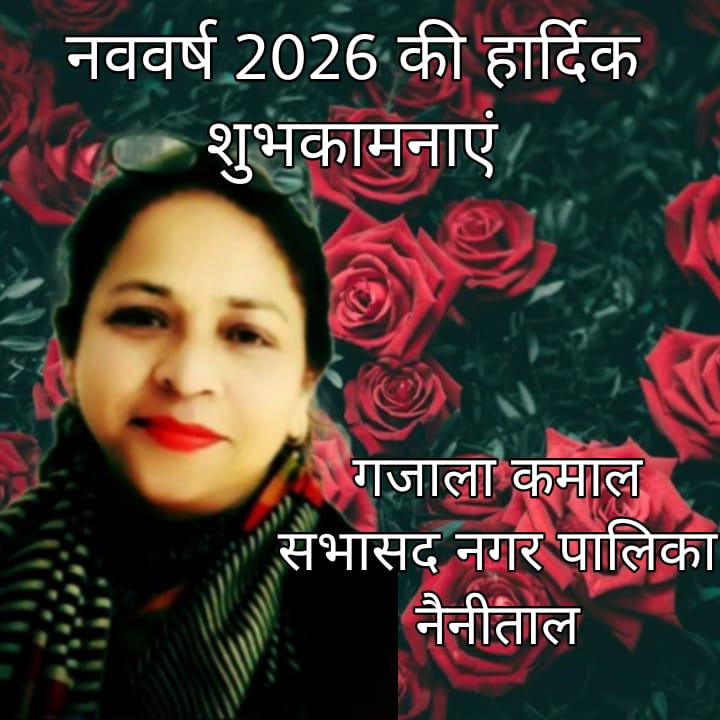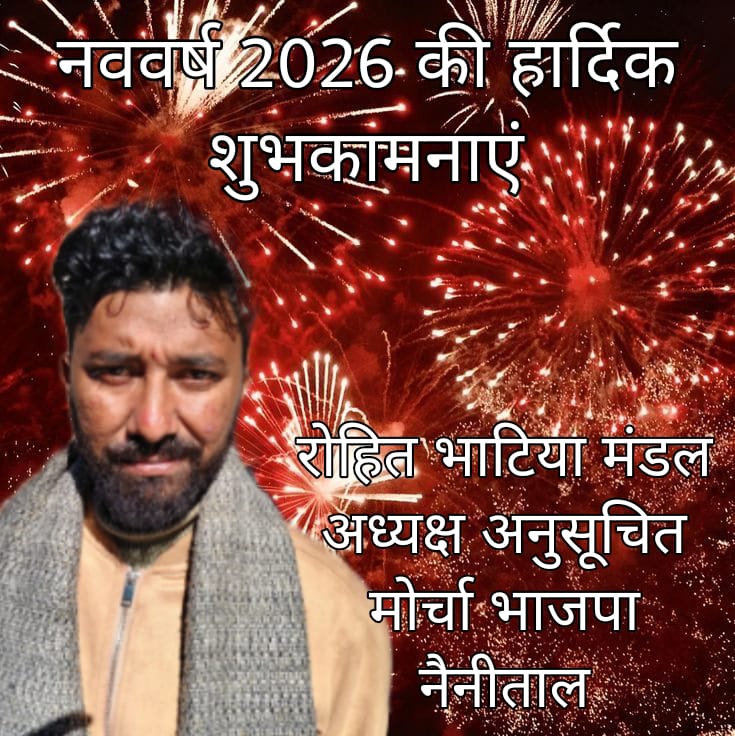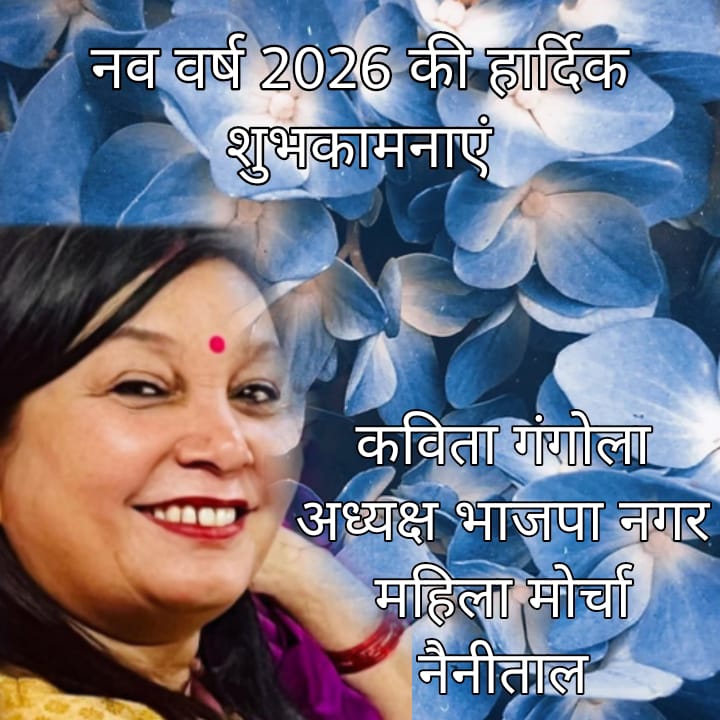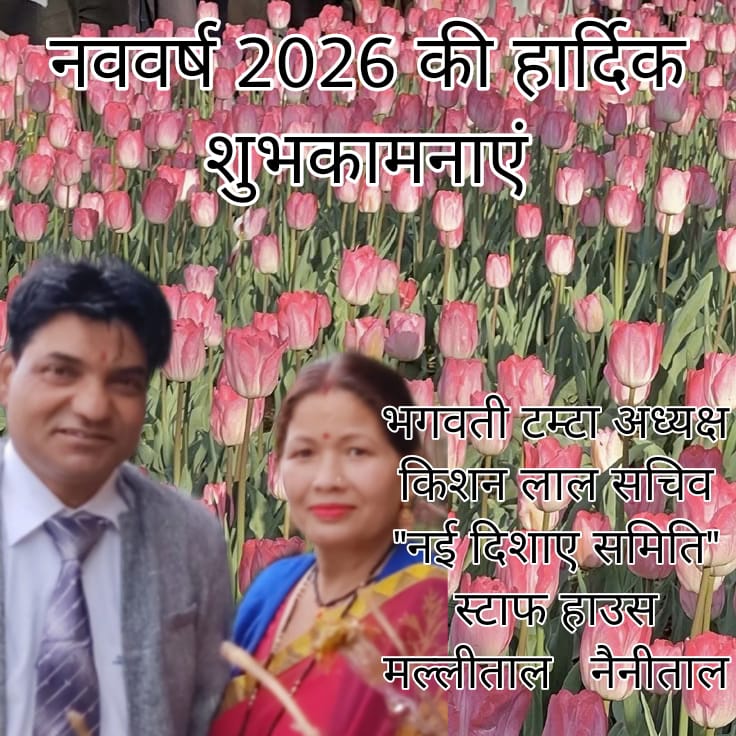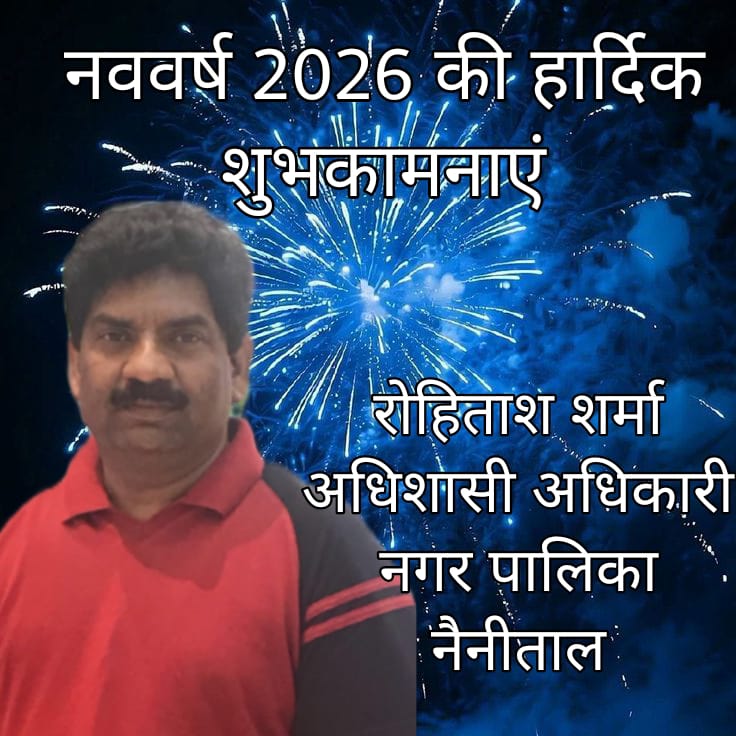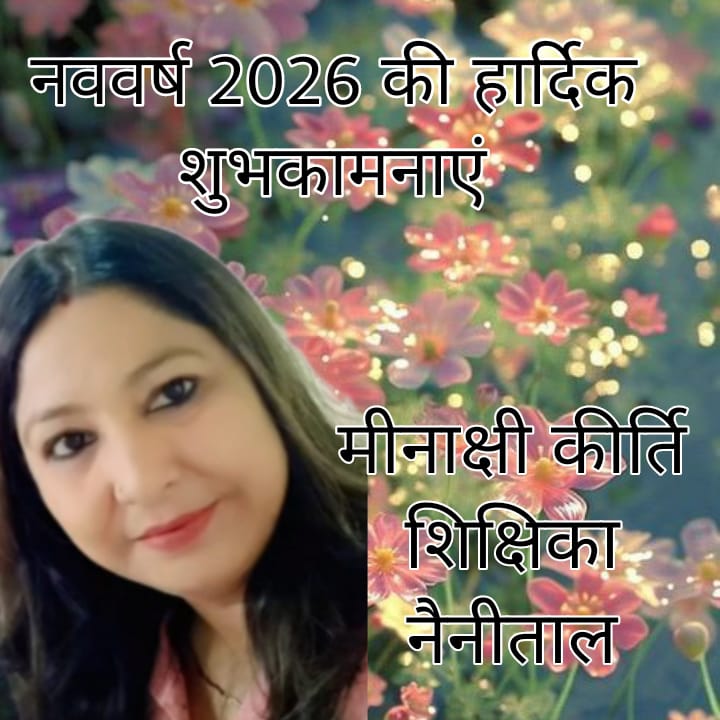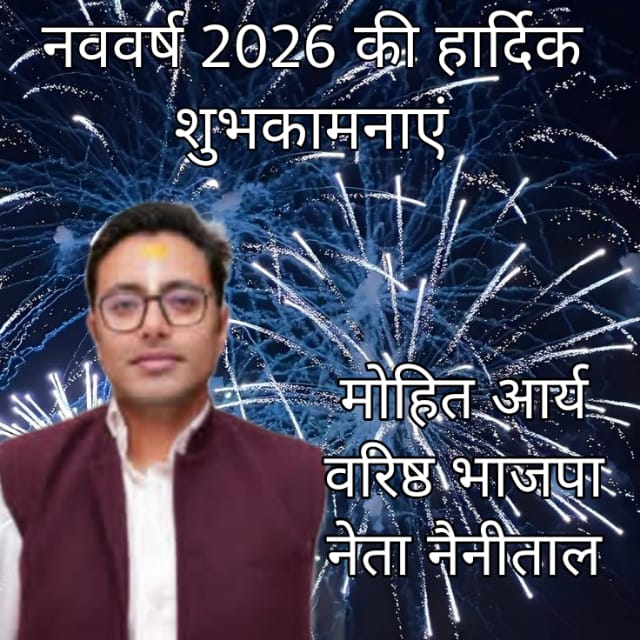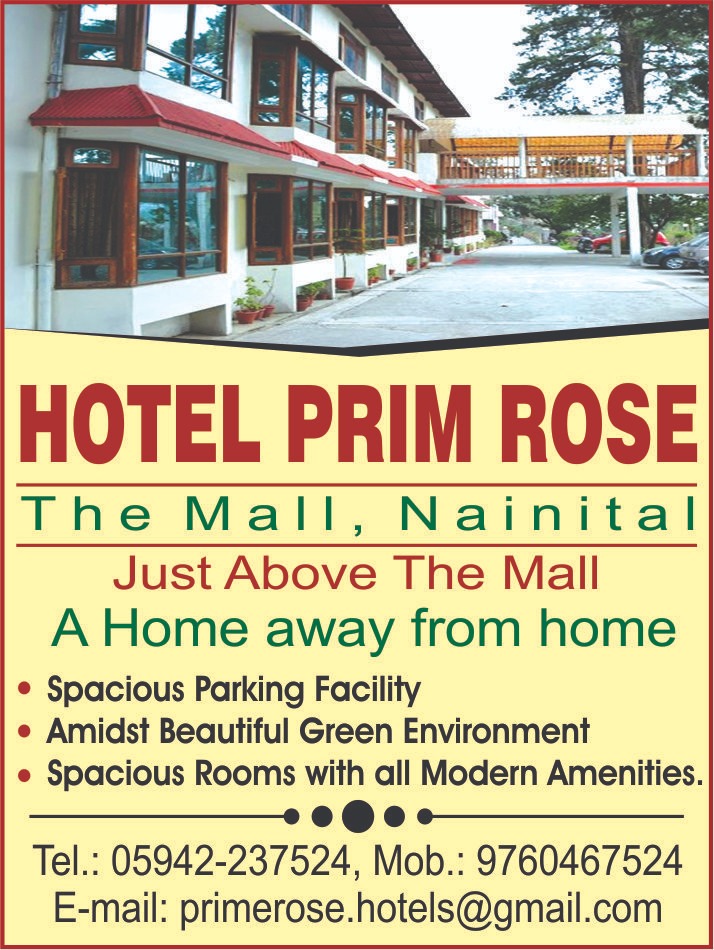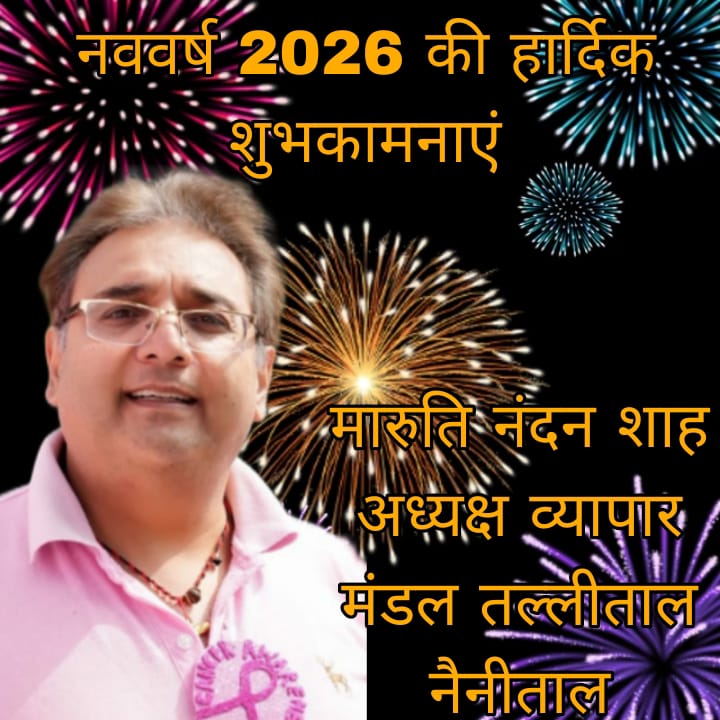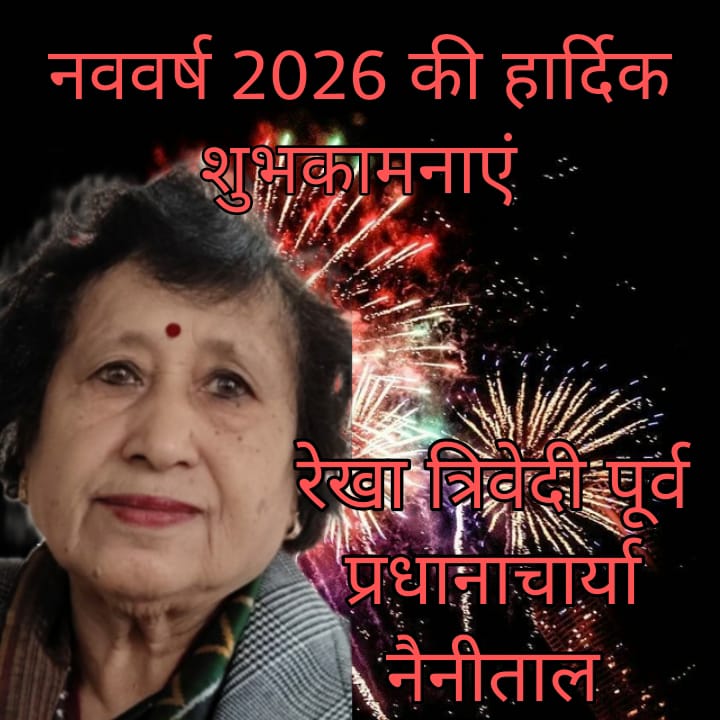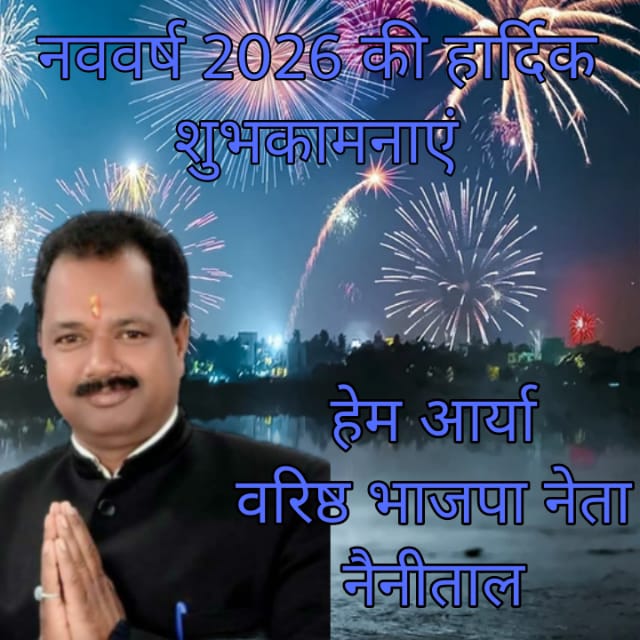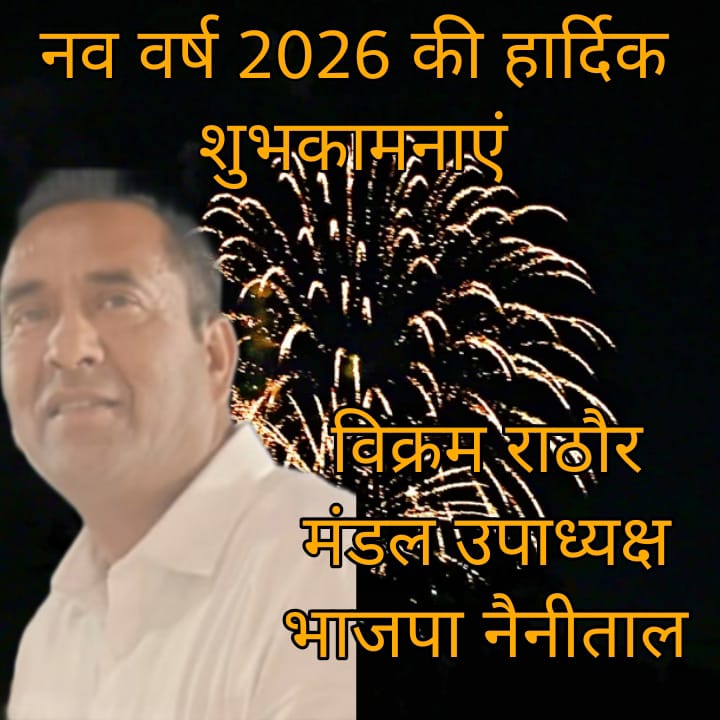अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन बादल फटने की घटनाओं पर हुई चर्चा
नैनीताल। डीएसबी परिसर के भूविज्ञान विभाग और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु की ओर से आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन बादल फटने की घटनाओं पर विशेषज्ञों ने की चर्चा की। सम्मेलन में इटली,अमेरिका, नेपाल और भारत के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। मंगलवार को डीएसबी के हर्मिटेज भवन में अयोजित की गई तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में देश व विदेश के आए हुए वैज्ञानिकों ने बादल फटने की घटनाओं पर चार्चा की। सम्मेलन में सभी विषेशज्ञों ने अपने शोध व अनुभवों को सांझा किया, कार्यक्रम का संचालन दिवाकर बवाड़ी ने किया। भूविज्ञान एवं भूभौतिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर के प्रो़ मनीष ए. ममतानी ने बताया की संरचनात्मक भूविज्ञान, पृथ्वी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में से एक है, जिसका ज्ञान विभिन्न भूविज्ञान परियोजनाओं, जैसे क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण, सतही एवं भूमिगत खनिज अन्वेषण/खनन, हाइड्रोकार्बन भंडार अध्ययन आदि में आवश्यक है। भारत 2047 तक एक ”विकसित राष्ट्र” बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए यह आवश्यक है कि भूवैज्ञानिक संरचनात्मक भूविज्ञान के मूल सिद्धांतों को उन क्षेत्रों में लागू करें जो समाज के लिए लाभकारी हों। स्वच्छ ऊर्जा, स्थिरता, महत्वपूर्ण खनिज और बुनियादी ढाँचा आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर काफी ध्यान केंद्रित कर रहा है। बांध, पुल, फ्लाईओवर, सुरंग जैसी बड़ी संरचनाएँ। इनके लिए संरचनात्मक भूविज्ञान और शैल यांत्रिकी का ठोस आधार आवश्यक है। किसी भी इंजीनियरिंग संरचना के लिए किसी स्थल की उपयुक्तता तय करने, प्रत्याशित समस्याओं की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए शैल शक्ति और उसकी विषमता, तथा सूक्ष्म संरचना के मूल सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ असाधारण हैं और आने वाले दशकों में कोयले और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को अंततः वैकल्पिक स्रोतों जैसे भूतापीय और परमाणु ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में भूवैज्ञानिक संरचनाओं, विभंजन जाल, सरंध्रता/पारगम्यता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे भारत अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू करेगा, यही ज्ञान-आधार गहन परमाणु अपशिष्ट निपटान के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण होगा। प्रो़ एसएस रावत ने कहा की हिमालय केवल प्रकृति की निर्मित दिवार नहीं है,बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, एक जलवायु नियामक, एक पारिस्थितिक ढाल और विशाल हिमखंडों का निवास स्थान है। हिमनदों और मानसून-जनित अपरदन निर्धारित होते हैं, जिससे ये तेज़ गति से बहने वाली, तलछट-समृद्ध और अत्यधिक गतिशील बनती हैं। युवा और नाज़ुक होने के कारण, ये नदियाँ भूवैज्ञानिक और जलवायु संबंधी शक्तियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अस्थिर, बाढ़-प्रवण और ख़तरे-प्रवण प्रणालियाँ बनती हैं। कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पीछे हट रहे हैं और आईपीसीसी एआर 6 के अनुसार उच्च तापमान की स्थिति में इस क्षेत्र के लगभग 65 फिसदी ग्लेशियर 2100 तक नष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार हिमालयी समुदायों की जीवन रेखा के रूप में काम करने वाले झरने खतरनाक दर से सूख रहे हैं। इसलिए, हॉटस्पॉट के जल-भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। इसके साथ ही विषेशज्ञों , वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने लगातार हो रही बादल फटनें की घटनाओं और कारकों पर चार्चा की इस दौरान प्रो़ जीएम भट्ट, संदीप रॉय, भोला नाथ ढाका, बीएस अरोरा,विपुल सिलवास, के चंद्रकला, नेकमल जाशी, महक, मनमाहन कौशल, धन बी तामंग, भाष्कर बिष्ट,आदि मौजूद रहे।